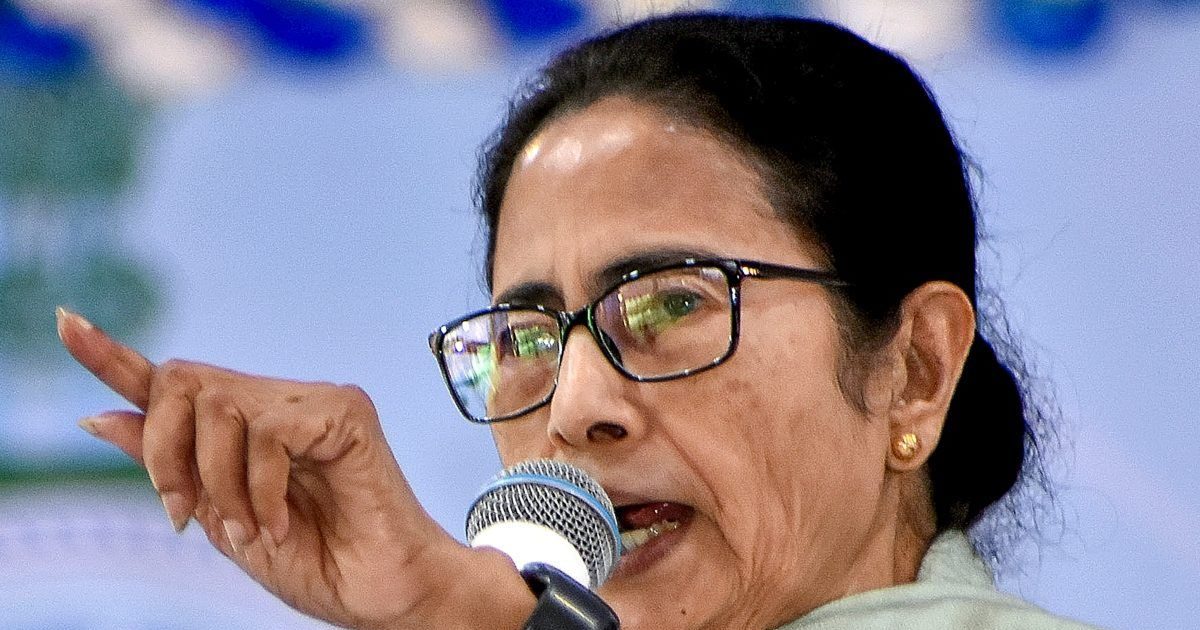Namdeo Dhasal Death Anniversary: कवि, चिंतक, विद्वान, सुधारक और राजनीतिक कार्यकर्ता. सबकुछ थे नामदेव ढसाल. 1950 के दशक में मुंबई के एक दलित परिवार में जन्मे ढसाल को उन हालातों से जूझना पड़ा, जो उस वक्त के कमोबेश तमाम दलितों की नियति में मानो लिख-सा दिया गया था- गरीबी, शोषण, शराब की लत. उनके बचपन के साल चोरों, दलालों, गैंगस्टर्स, सेक्स वर्कर्स और ड्रग्स बेचने वालों के साथ पुलिस से भागते बीते थे. इसलिए भी उनकी कविताओं में जहां विषम परिस्थितियों के प्रति एक आक्रोश नजर आता है तो वहीं इसी आक्रोश को स्वर देने के लिए वे राजनीति को एक हथियार के तौर पर आजमाने से भी पीछे नहीं रहे.
महाराष्ट्र में ढसाल की पहचान एक कवि से भी ज्यादा एक राजनीतिक विचारक और कार्यकर्ता की रही है. वे अमेरिका की ब्लैक पैंथर्स पार्टी से बेहद प्रभावित थे, जो अश्वेत लोगों को सदियों से जारी पुलिस बर्बरता और भेदभाव से बचाने के लिए कार्य कर रही थी. इसी से प्रेरित होकर ढसाल ने तत्कालीन बॉम्बे की झुग्गियों में जून 1972 में दलित पैंथर आंदोलन की शुरुआत की. इस आंदोलन की नीतियां कार्ल मार्क्स और डॉ. भीमराव अंबेडकर से प्रेरित थीं. कवि-क्रांतिकारी जेवी पवार, राजा ढाले और अर्जुन दांगले उस दलित पैंथर आंदोलन के अन्य संस्थापक सदस्य थे. उनके इस दलित आंदोलन ने खासकर युवाओं को आकर्षित किया और उन्होंने अपनी कविताओं, लेखों और जमीनी स्तर की सक्रियता के जरिए बदलाव लाने की कोशिश की.
दलित पैंथर आंदोलन का उभार भारतीय संविधान के निर्माता डॉ बी.आर. अंबेडकर के निधन के बाद उपजी परिस्थितियों का भी नतीजा था. दरअसल, 1956 में अंबेडकर के निधन के बाद उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हालत खस्ता हो गई थी. खुद को दलित नेता कहने वाले कई लोगों ने राजनीति में टिके रहने के लिए उन ताकतों से हाथ मिला लिए, जिनका अंबेडकर हमेशा से विरोध करते रहे थे. 1966 तक महाराष्ट्र में एक नए संगठन शिवसेना का उदय भी हो चुका था, जिसने दक्षिण भारतीयों, साम्यवादियों, मुस्लिमों और यूपी-बिहार के लोगों के खिलाफ अपने हिंसक आंदोलन, दुर्व्यवहार और आक्रामकता को अपनी पहचान बना लिया था. कट्टर हिन्दू संस्कृति से पोषित इस राजनीति ने अंबेडकर के अनुयायियों को असहज कर दिया और वे बेसब्री से कोई ऐसा मंच तलाशने लगे, जहां समानता और आजादी की उनकी आवाज मुखर हो सके. उनके लिए ‘दलित पैंथर्स’ ऐसा ही मंच बना.
गांव-गांव में बना ली थी पहचान…
1972 से 1977 के बीच दलित पैंथर्स ने अपनी एक जगह बना ली और उसके सदस्य आत्म-सुरक्षा के गुर सीखने लगे ताकि समुदाय के खिलाफ अत्याचारों का जवाब दे सकें. दलित पैंथर्स के सदस्य उन गांवों में जाते जहां अत्याचार की घटनाएं होतीं और विरोध प्रदर्शन करते. इस तरह उन्होंने मुंबई के माटुंगा, दादर, चेंबूर, घाटकोपर, शिवडी, परेल और वर्ली में अपने प्रभाव वाले इलाके बना लिए. 1973 में दलित पैंथर्स ने बाकायदा एक घोषणापत्र जारी करके मार्क्सवादी सोच एवं बौद्ध धर्म को एक-दूसरे का पूरक और जमींदारों, उद्योगपतियों, सूदखोरों और सरकार को दलितों का दुश्मन करार दिया. दलित शब्द का दायरा भी बढ़ाया गया, ताकि अनुसूचित जातियों के अलावा नव बौद्ध, भूमिहीन गरीब किसानों और शोषित महिलाओं जैसे दबे-कुचले वर्गों को इसमें शामिल किया जा सके. दलित पैंथर्स के अभियानों में कविता एक शक्तिशाली हथियार हुआ करती थी. कुछ ही महीनों में शहर के विभिन्न हिस्सों में संगठन की 30 से ज्यादा इकाइयां खुल गईं. जब नुक्कड़ सभा के जरिए विरोध प्रदर्शन होते तो ये इकाइयां कविता पाठ और लघु कथा पाठ के सत्र रखतीं.
राजनेता के तौर पर विफल रहे…
निर्वाचित प्रतिनिधि के संदर्भ में बात करें तो ढसाल जनता के बीच बतौर राजनेता सफल नहीं रहे. उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं जीता, बल्कि अपने कुछ प्रयोगों और समझौतों की वजह से उन्होंने अपने लिए आलोचनाओं के दरवाजे भी खोल लिए. उनकी आलोचनाएं राजनीतिक कुटिलता का अभाव ही दर्शाती हैं. उदाहरण के तौर पर, अपने ही बनाए समूह को तोड़ने का फैसला, अपनी कविता और कृत्यों दोनों के जरिये इंदिरा गांधी की प्रशंसा और बाद में बालासाहेब ठाकरे की उस शिवसेना के साथ गठबंधन की कोशिश करना, बतौर संगठन जिससे उन्हें हमेशा चिढ़ रही.
हालांकि ढसाल के प्रति सहानुभूति रखने वालों का कहना है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को समर्थन देने का उनका फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अदालतों में चल रहे मामले रद्द कराने की जरूरत से जुड़ा था. जून 1975 में जब आपातकाल लगाया गया, तब ढसाल के नेतृत्व में दलित पैंथर्स ने पुरजोर विरोध किया. लेकिन अक्सर हिंसक हो जाने वाला उनका तरीका महंगा साबित हुआ. ढसाल समेत अन्य दलित पैंथर्स नेताओं के खिलाफ करीब 200 मामले दर्ज हो गए. आगे चलकर शिवसेना के साथ गठबंधन की कोशिश की वजह से भी ढसाल को आलोचनाएं झेलनी पड़ीं. ढसाल का मानना था कि शिवसेना के साथ गठबंधन करने से दलितों को मुख्यधारा की राजनीति में आने में मदद मिलती. लेकिन उनका ये कदम उन पर ही भारी पड़ गया और शिवसेना भी राज्य चुनाव में उन्हें टिकट देने के अपने वादे से मुकर गई.
‘जब मैंने नियमों की सारी किताबें बाहर फेंक दीं’…
ढसाल बेहद गरीबी में पले-बढ़े और स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर सके. वे कभी कॉलेज नहीं जा सके, लेकिन खुद जितना हो सका पूरे उत्साह के साथ पढ़ा. यहां तक कि टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए, लंबा इंतजार करते या रुकते जब समय मिलता, वह अक्सर पढ़ा करते थे. एक बार उन्होंने अपने जीवन के एक हिस्से का उल्लेख इन शब्दों में किया है: ‘मैंने नशा किया. वेश्यालयों में गया. मुजरा करने वाली औरतों के पास गया और साधारण वेश्याओं के घर भी गया. ये पूरा माहौल और इसकी प्रकृति जीवन का अलग ही रूप उजागर करती थी. ये जीवन था! फिर मैंने नियम की सभी किताबें बाहर फेंक दीं. अब मेरे लिए छंद लिखने के कोई नियम नहीं थे. मेरी कविता उतनी ही स्वतंत्र थी, जितना मैं था. मैंने वही लिखा, जैसा मुझे लगा कि लिखना चाहिए.’
भक्ति संत-कवि तुकाराम से भी की गई तुलना…
ढसाल के पिता लक्ष्मण ढसाल खेड तालुक के गांव पुर-कनेरसर से मुंबई आए थे. तमाम प्रवासियों की तरह महानगर में ढसाल के लिए रहने की पहली जगह गोलपिठा थी, जो रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा से सटी थी. वहीं उनके पिता एक कसाई के साथ काम करते थे. बाद में ढसाल ने अपने पहले और सबसे ज्यादा पसंदीदा कविता संग्रह का नाम ‘गोलपिठा’ रखा.
उनके बचपन के दिनों के परिवेश का प्रभाव गोलपिठा में पूरी तरह झलकता है, जो 1971 में प्रकाशित हुआ. इसने उन्हें प्रतिष्ठित सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिलवाया. मराठी साहित्य में ढसाल की उपलब्धियों के लिए 1999 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया. साल 2004 में साहित्य अकादमी ने उन्हें गोल्डन लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया.
द्विभाषी लेखक, अनुवादक, संपादक और आलोचक प्रोफेसर सचिन केतकर कहते हैं कि दूसरे दलित लेखकों से ढसाल को जो चीज अलग करती थी, वो है भाषा के इस्तेमाल में नयापन लाने की उनकी कला. मराठी नाटककार और आलोचक विजय तेंदुलकर ने ढसाल की तुलना महाराष्ट्र के ख्यात भक्ति संत-कवि तुकाराम से की है. ढसाल के आखिरी छह महीने अस्पताल में बीते. कोलन कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद शारीरिक दुर्बलता के कारण 15 जनवरी 2014 को 64 वर्ष की आयु में मुंबई में ढसाल का निधन हो गया.

 4 weeks ago
4 weeks ago










)