एक शाम गांव में टहलते हुए बंकिमचंद्र चटोपाध्याय प्रकृति की सुंदर छटा देखकर इतने मुग्ध हो गए कि तुरंत कलम निकाली और फटाफट वंदेमातरम गाने की चार लाइनें लिख डालीं. हालांकि इसके बाद उन्होंने इसे कई बार बदला और कई सालों में पूरा किया. इस गीत की यात्रा भी बहुत रोचक है.
इतिहासकारों के अनुसार बंकिमचंद्र चटोपाध्याय ने पहली बार 7 नवंबर 1875 में वंदेमातरम को सार्वजनिक रूप से एक साहित्यिक गोष्ठी में सुनाया. इसके बाद ये कविता बहुत तेजी से लोकप्रिय होती चली गई. खासकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे सेनानियों के लिए ये हमेशा उनकी जुबान पर रहने वाला गाना बन गया. हर क्रांतिकारी इसे गाते हुए जोश जगाने का काम करता था. धीरे धीरे ये पूरे देश में गाया जाने लगा. कह सकते हैं कि आजादी की पूरी लड़ाई में ये राष्ट्रीय चेतना का गीत बन गया.
कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया
“वंदे मातरम्” गीत को 1896 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, उस मंच पर ये गीत किसी और ने नहीं बल्कि रवींद्रनाथ टैगोर ने गाया. जब इस गीत की रचना की गई तब बंकिमचंद्र नदिया ज़िले में डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे थे. बाद के बरसों में 7 नवंबर को वंदे मातरम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. इस बार इसके 150 साल पूरे हो रहे हैं.
बंकिम चंद्र चटर्जी का 1872 में लिखा एक गीत कालजयी रचना बना और ये पूरे देश में आजादी की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय चेतना का स्वर बनकर उभरा. (विकी कामंस)
7 नवंबर 1905 को कोलकाता में “वंदे मातरम्” के नारों से भरा विशाल जुलूस तब निकाला गया, जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया. तब ये गीत प्रतिरोध गान बनकर पूरे बंगाल में उभरा.
कैसे इस गीत के भाव मन में आए
बंकिमचंद्र नदिया ज़िले के कांतलपाड़ा गांव में एक दिन शाम को टहल रहे थे, तभी मंद-मंद चलती हवा और हरियाली से लहराती धरती को देखकर उनके मन में मातृभूमि के प्रति गहरा भाव उमड़ा, उन्होंने अपनी नोटबुक में तुरंत लिखा –
“वंदे मातरम्…” यह केवल 3-4 पंक्तियों का छोटा गीत था, जिसमें भारत को मां के रूप में पुकारा गया था.
इतिहासकारों के अनुसार, वंदेमातरम का ये शुरुआती संस्करण “बंगला मिश्रित संस्कृत” में था. इसमें केवल मातृभूमि के सौंदर्य का वर्णन था, कोई धार्मिक या दुर्गा-प्रतीक नहीं.
दोबारा कब इसे बदला और विस्तार दिया
अपने इस गीत को उन्होंने 1875 में फिर बदला और विस्तार दिया. इसे उनके इस गीत का दूसरा संस्करण कहा जा सकता है. तब वह बंगाल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति से व्यथित थे. वह चाहते थे कि कोई गीत भारतवासियों में आत्मगौरव जगाए. इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी पंक्तियों को फिर से देखा और विस्तार दिया –
अब उन्होंने “मां” को “भारत माता” और “देवी” दोनों रूपों में चित्रित किया. इस संस्करण में संस्कृत के श्लोक-जैसे शब्द आए.
“त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी…” यानी यह गीत देशभक्ति और भक्ति दोनों के मिश्रण में बदल गया.
फिर इसके तीसरे संस्करण की रचना की
बंकिम चंद्र चटोपाध्याय ने इस गीत को फिर कुछ बदला और अंतिम रूप दिया. इसके पूरे स्वरूप को उन्होंने तीसरा और अंतिम रूप : “आनंदमठ” (1881–1882) में रखा. आनंद मठ उनका उपन्यास था. जो 1881-82 में प्रकाशित हुआ. उनका ये उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ. उन्होंने ये गीत अपने उपन्यास में इसलिए रखा क्योंकि उन्हें लगा कि बरसों पहले उन्होंने वंदेमातरम के रूप में जो गीत लिखा है, उसको उपन्यास में पात्रों के माध्यम से गवाया जाए.
“आनंदमठ” में ये गीत साधु-सैनिकों के विद्रोह के समय गाया जाता है, जो मातृभूमि को देवी रूप में पूजते हैं. यहां उन्होंने गीत को अंतिम रूप दिया – कुल 12 श्लोकों में. हालांकि बाद में जब राष्ट्रगीत के रूप में इसे लिया गया, तो केवल पहले दो श्लोक स्वीकार किए गए, क्योंकि बाकी के श्लोक देवी-पूजा के संदर्भ में थे.
बंकिमचंद्र ने इसे कब कब और कैसे बदला
ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, उन्होंने कम से कम तीन बार इसमें बदलाव किया.
1. पहला संस्करण (1872–73) – मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन
2. दूसरा संस्करण (1875–76) – भारतमाता को देवी के रूप में पेश किया, संस्कृत के शब्द जोड़े
3. तीसरा (अंतिम) संस्करण (1881–82) – कोलकाता में रहकर आनंदमठ उपन्यास लिखने के दौरान . तब इसे 12 पदों वाला पूर्ण गीत बनाया.
ये कह सकते हैं कि इस गीत का शुरुआती रूप उन्होंने उन्होंने एक ही शाम में लिखा लेकिन इसको अंतिम स्वरूप तक पहुंचने में 8–10 साल लग गए.
क्या बंकिम चंद्र ने कोई और कालजयी गीत लिखा
उन्होंने कई प्रसिद्ध गीत लिखे लेकिन वो वंदे मातरम् जितने प्रसिद्ध नहीं रहे. “आनंदमठ” और “देवी चौधरानी” जैसे उपन्यासों में उन्होंने कई और गीत भी लिखे, जैसे “मां, तुझ पर प्राण निछावर.” लेकिन वंदेमातरम जैसा जनांदोलन बन जाना किसी और गीत के साथ नहीं हुआ.
क्या बंकिमचंद्र अंग्रेज़ सरकार की नौकरी करते रहे?
हां, पूरे जीवन वह ब्रिटिश सरकार की सेवा में रहे. हालांकि उनके मन में राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान की ज्वाला जलती रही. 1858 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली. वह पहले भारतीय स्नातकों में एक थे. उसी वर्ष ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस (ICS) के जरिए वह डिप्टी मजिस्ट्रेट और फिर डिप्टी कलेक्टर बने. उन्होंने 24 साल तक (1858–1891) बंगाल के अलग-अलग जिलों जैसे नदिया, जेसोर, हुगली, मिदनापुर में सेवा की.
खास बात ये थी कि वे नौकरी के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कह सकते थे, पर अपने लेखन के जरिए उनका विरोध दर्ज कराते रहे. आनंदमठ” के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन को परोक्ष रूप से चुनौती दी. उसमें “सन्यासी विद्रोह” दरअसल ब्रिटिश शासन के दमन के खिलाफ एक प्रतीक था. उनकी कृति “कृष्णचरीत्र” में भी उन्होंने धर्म, नीति और आत्मबल को स्वतंत्रता की जड़ बताया।
क्या अंग्रेज़ सरकार को उन पर शक हुआ था?
हां, हुआ था. “आनंदमठ” के प्रकाशन (1882) के बाद ब्रिटिश अफसरों ने महसूस किया कि यह उपन्यास राजद्रोही भावना फैला सकता है, क्योंकि उसमें सशस्त्र साधुओं द्वारा अंग्रेज़ शासन का विरोध दिखाया गया था. लेकिन चूंकि बंकिमचंद्र ने इसे सीधे तौर पर ब्रिटिश-विरोधी नहीं लिखा बल्कि धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से कहा, लिहाजा सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकी.
उन्होंने 1891 में सरकारी सेवा से अवकाश लिया. 1894 में उनकी मृत्यु हो गई, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष, सुभाषचंद्र बोस सभी ने माना कि “अगर बंकिम न होते, तो ‘भारत माता’ का विचार इतना जीवंत रूप न ले पाता.”
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

 1 month ago
1 month ago
)
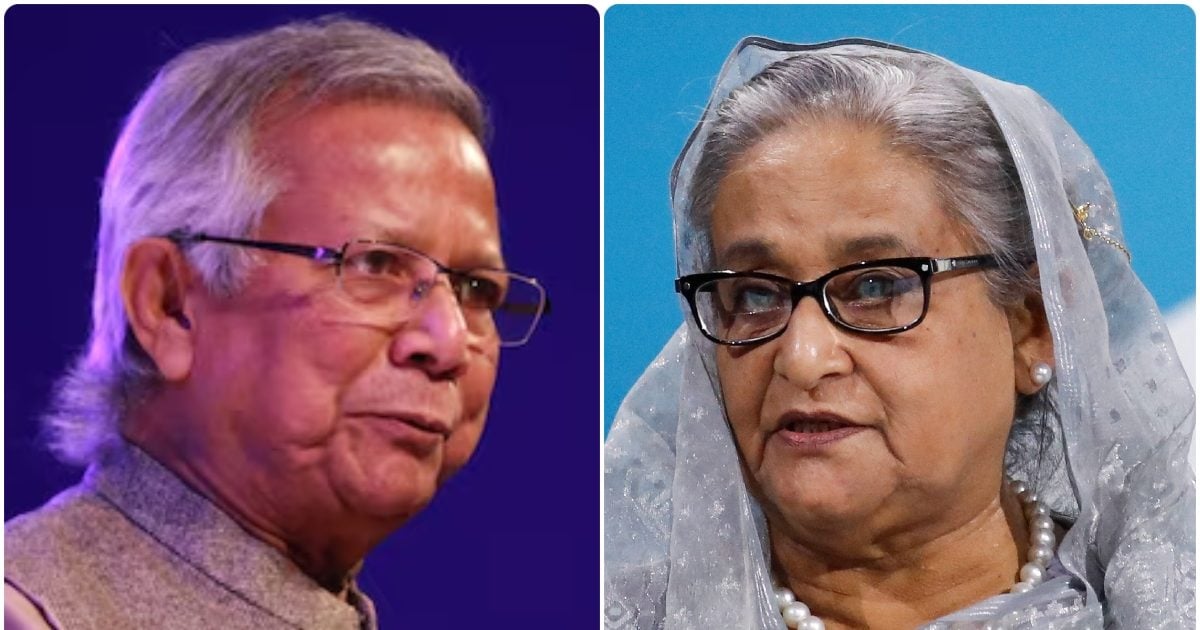



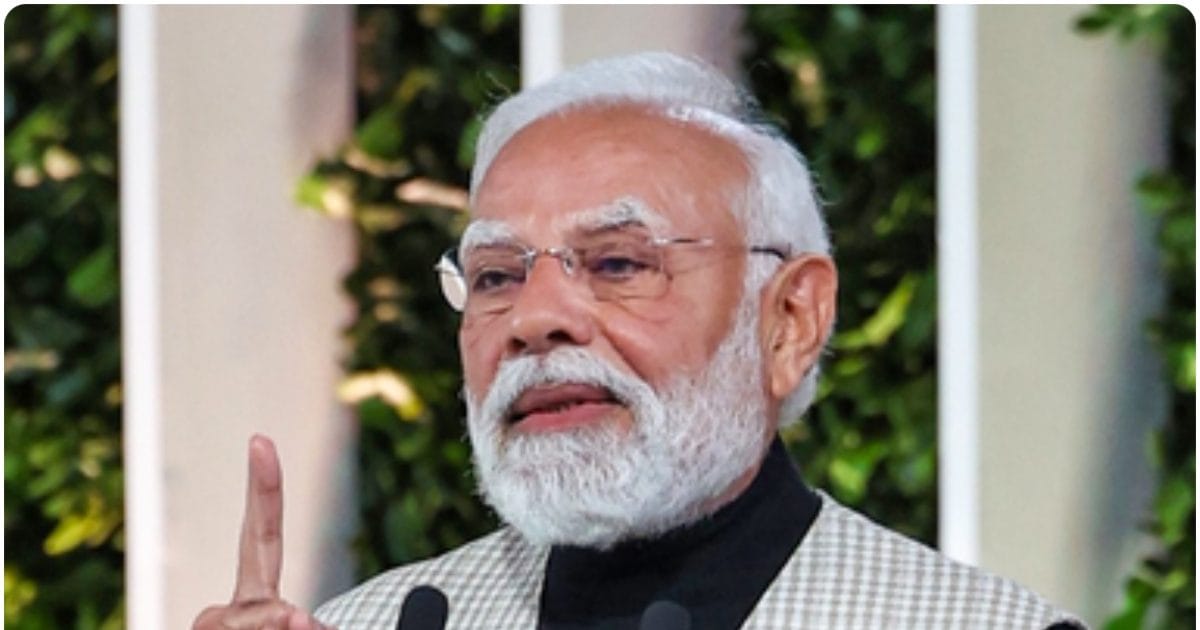


)
)
)
)



