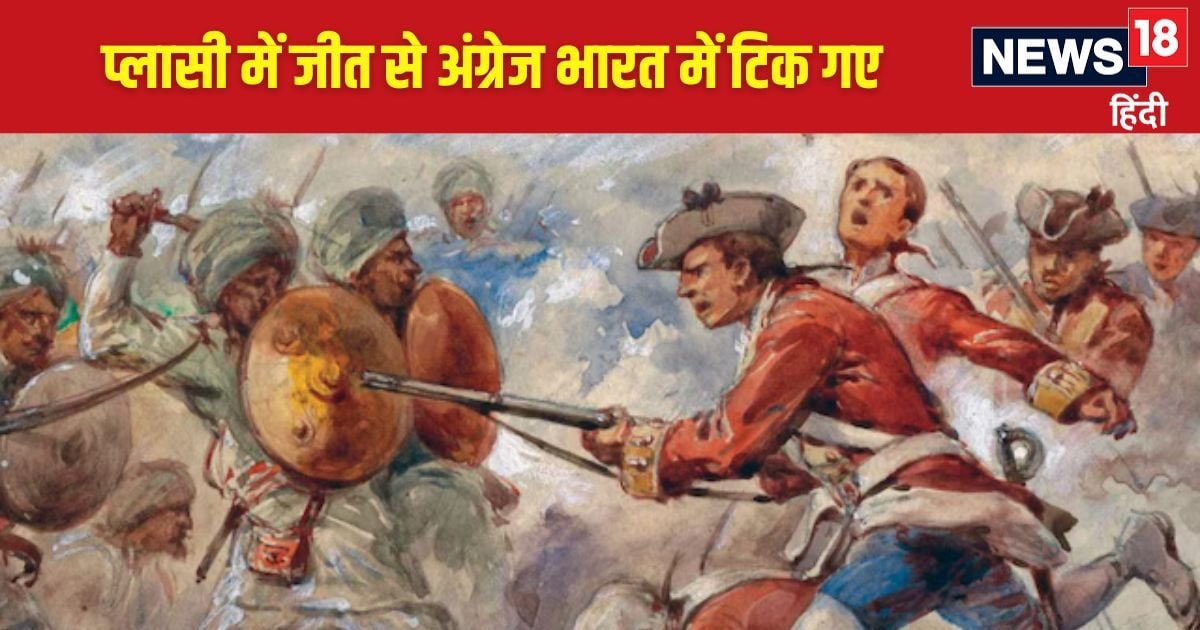भारत और पाकिस्तान के बीच घोषित तौर पर तीन युद्ध हो चुके हैं. दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष फिर से चल रहा है. हालांकि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है. कैसे एक देश दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है और फिर क्या होता है.
जब कोई देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है, तो यह एक औपचारिक और गंभीर कदम होता है, जिसके कई राजनैतिक, कानूनी, सैन्य और सामाजिक परिणाम होते हैं.
सवाल – कैसे कोई देश करता है युद्ध की घोषणा, क्या इसकी कोई प्रक्रिया है?
– युद्ध की घोषणा आमतौर पर देश की सरकार या शीर्ष नेतृत्व द्वारा की जाती है. यह संसद, राष्ट्रपति, या समकक्ष प्राधिकरण के जरिए होती है. घोषणा में साफतौर पर युद्ध की वजहों, लक्ष्य और विरोधी देश का उल्लेख होता है. हालांकि भारत ने कई युद्ध लड़े हैं लेकिन संसद में इसकी मंजूरी एक ही बार 1971 में ली गई. हर बार प्रधानमंत्री ने ही इसकी घोषणा कर दी.
हालांकि कई देशों में युद्ध के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है. युद्ध की घोषणा एक लिखित दस्तावेज के रूप में की जा सकती है, जिसे दूसरे देश को सौंपा जाता है. इसमें युद्ध की वजहों को स्पष्ट किया जाता है. युद्ध की स्थिति में दोनों देश एक-दूसरे के राजनयिकों (दूतावास कर्मचारियों) को वापस बुला सकते हैं.
सवाल – भारत ने अब तक जो युद्ध लड़े हैं, उसमें उसने कैसे इसकी घोषणा की है, कितनी बार संसद की मंजूरी ली गई?
– भारत ने अब तक जितने भी युद्ध लड़े हैं, उनमें से अधिकांश मामलों में औपचारिक रूप से संसद की मंजूरी के बिना ही सैन्य कार्रवाई की गई. हालांकि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352-360 (आपातकालीन प्रावधान) और रक्षा नीतियों के तहत सरकार को युद्ध जैसी स्थितियों में विशेष अधिकार प्राप्त हैं.
1. 1947-48 का भारत-पाक युद्ध (कश्मीर युद्ध)
घोषणा – कोई औपचारिक युद्ध घोषणा नहीं
कारण – पाकिस्तानी कबायलियों द्वारा कश्मीर पर आक्रमण के बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई की
संसद की भूमिका – तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सीधे सेना को आदेश दिया, संसद से पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया.

भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद की कोई मंजूरी नहीं ली थी. (News18 AI)
2. 1962 का भारत-चीन युद्ध
घोषणा – कोई युद्ध घोषणा नहीं, चीन ने अचानक आक्रमण किया.
संसद की प्रतिक्रिया – युद्ध के दौरान संसद में चर्चा हुई, पोस्ट-फैक्टो (बाद में) मंजूरी दी गई.
विशेष तथ्य – तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन संसद से पहले अनुमोदन नहीं लिया.
3. 1965 का भारत-पाक युद्ध
घोषणा – पाकिस्तान ने पहले “ऑपरेशन जिब्राल्टर” का छुपा हमला किया, भारत ने जवाबी कार्रवाई की
संसदीय प्रक्रिया – 3 सितंबर 1965 को संसद ने “आक्रमण का सामना करने” के लिए प्रस्ताव पारित किया. यह औपचारिक युद्ध घोषणा नहीं थी, बल्कि सरकार को समर्थन देने वाला प्रस्ताव था. तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को खुली छूट दी.

1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की बैठक बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव पारित किया. यह भारत के इतिहास में संसद द्वारा युद्ध को मंजूरी देने का अकेला उदाहरण है. (फाइल फोटो)
4. 1971 का भारत-पाक युद्ध (बांग्लादेश मुक्ति संग्राम)
घोषणा – 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्र पर हमला किया, भारत ने औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति घोषित की.
संसद की भूमिका – 4 दिसंबर 1971 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया. दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) ने सर्वसम्मति से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव पारित किया. यह भारत के इतिहास में संसद द्वारा युद्ध को मंजूरी देने का सबसे साफ उदाहरण है.
परिणाम – भारत की जीत, बांग्लादेश का उदय.
5. 1999 का कारगिल युद्ध
घोषणा – कोई युद्ध घोषणा नहीं, पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ “ऑपरेशन विजय” चलाया गया.
संसद की प्रतिक्रिया -संसद ने एकमत से पाकिस्तान की निंदा की, लेकिन युद्ध की औपचारिक मंजूरी नहीं दी. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे सेना को निर्देश दिए. कारगिल संघर्ष में युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसे “सैन्य ऑपरेशन” कहा गया.
सवाल – वैसे भारत में भारत में युद्ध घोषणा की कानूनी प्रक्रिया क्या है?
– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति (सरकार की सलाह पर) सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है. अनुच्छेद 352 (आपातकाल) में संसद की मंजूरी जरूरी है, लेकिन युद्ध शुरू करने के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है. युद्ध जैसी स्थिति में सरकार संसद को सूचित करती है, लेकिन पूर्व अनुमोदन जरूरी नहीं है. रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट की सुरक्षा समिति (CCS) फैसला लेती है.
सवाल – क्या इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया भी होती है?
– कई देशों में युद्ध की घोषणा के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है. उदाहरण के लिए, संसद या विधायिका की मंजूरी आवश्यक हो सकती है. यह अंतरराष्ट्रीय कानून, जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत भी जांचा जा सकता है. युद्ध अपराध के मामले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICC) में जा सकते हैं, जैसा इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रूसी प्रेसीडेंट व्लादीमीर पुतिन के खिलाफ हुआ है.
सवाल – युद्ध की घोषणा के बाद क्या होता है?
– सेनाएं सक्रिय हो जाती हैं, सीमाओं पर तैनाती बढ़ जाती है. दुश्मन देश के खिलाफ हवाई हमले, जमीनी आक्रमण या नौसैनिक घेराबंदी शुरू हो सकती है.
UN और अन्य देश युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता (Mediation) कर सकते हैं. कुछ देश तटस्थ रह सकते हैं या किसी एक पक्ष का समर्थन कर सकते हैं.
सवाल – क्या युद्ध लड़ने वाले देशों पर आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं?
– हां, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में रूस के खिलाफ तमाम प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा लगाए गए हैं. व्यापार, निवेश और यात्रा प्रतिबंधित हो सकते हैं.
सवाल – क्या आजकल युद्ध की औपचारिक घोषणा होती है?
– आधुनिक समय में देश बिना औपचारिक घोषणा के भी सैन्य कार्रवाई करते हैं. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब भी युद्ध की बजाए स्पेशल मिलिट्री आपरेशन के तौर पर संबोधित किया जा रहा है. बेशक सारी दुनिया उसको युद्ध कह रही हो.
सवाल – युद्ध के दौरान किस अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाता है?
– युद्ध के दौरान जिनेवा संधि जैसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है, जो युद्धबंदियों, नागरिकों और मानवीय सहायता की सुरक्षा से संबंधित हैं.

 1 month ago
1 month ago

)


)

)

)