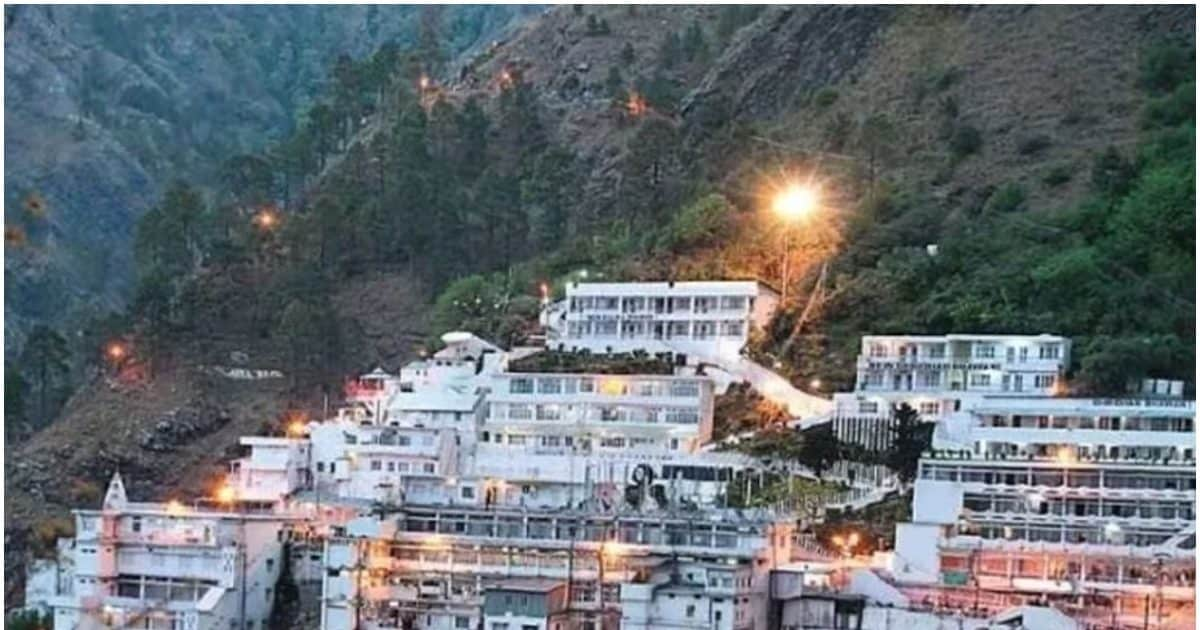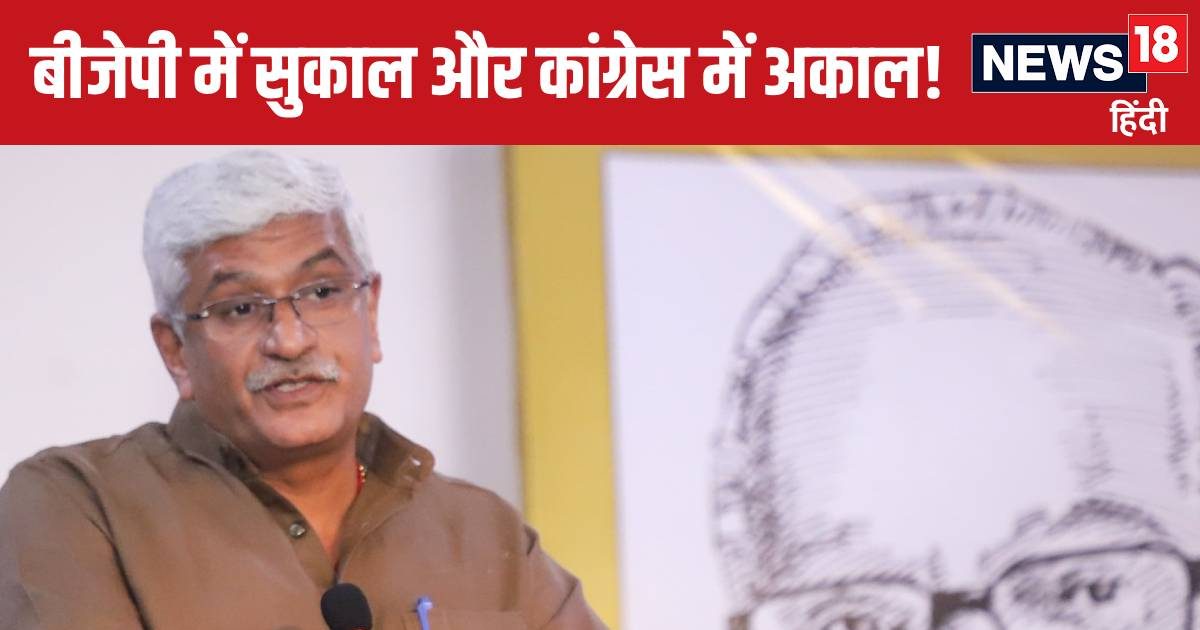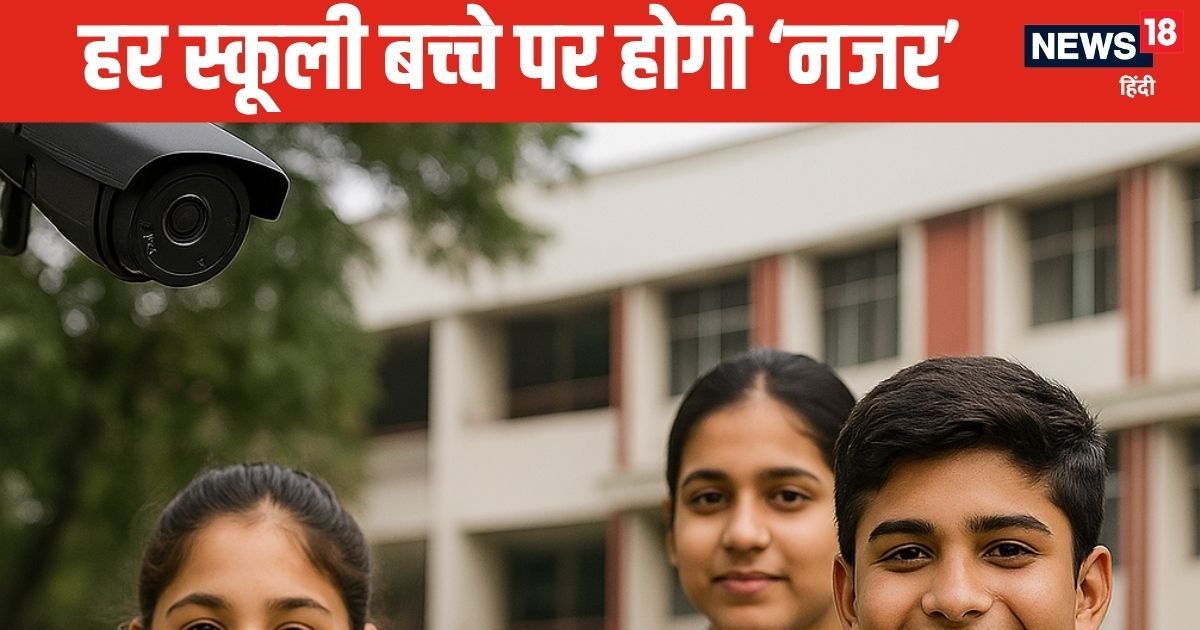नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल समेत देश के 7 सबसे बिजी रेलवे स्टेशनों पर फेशियल रिकॉग्रिशन तकनीक को लागू कर दिया है. हालांकि भारत के कई हवाईअड्डों समेत कई जगहों पर ये तकनीक पहले से लागू है. सरकार का कहना है कि रेलवे स्टेशनों पर इस तकनीक के लागू होने के बाद सुरक्षा को और बेहतर किया जा सकेगा. चीन जैसे देश में ये तकनीक चौराहों से लेकर हर जगह लागू है. वैसे इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी गिनाए जाते हैं.
फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक यानि एफआरटी(FRT) का इस्तेमाल दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहा है. एक हालिया अध्ययन के अनुसार, लगभग 100 से अधिक देशों में यह तकनीक अलग अलग जगहों पर लागू की जा रही है.
कॉम्पैरटेक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के 40% देशों में कार्यस्थलों पर FRT का उपयोग हो रहा है, जबकि 24% देशों में कुछ बसों और करीब 40% देशों में कुछ ट्रेनों और मेट्रो में यह तकनीक लागू है.
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देश जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, और फ्रांस में FRT का उपयोग हवाई अड्डे, पुलिस निगरानी, सार्वजनिक परिवहन, और निजी क्षेत्रों में देखा जा रहा है
सवाल – फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक क्या है?
फेशियल रिकॉग्निशन (चेहरे की पहचान) एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं का विश्लेषण करके उसकी पहचान करती है. यह तकनीक डिजिटल छवियों या वीडियो फ्रेम में चेहरे में आंखों, नाक, मुंह और चेहरे की संरचना को स्कैन करती है. इसे डेटाबेस में मौजूद जानकारी से मिलान करती है. यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर आधारित होती है.
सवाल – भारत में 7 रेलवे स्टेशनों पर फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक क्यों लागू की जा रही है?
– भारतीय रेलवे ने सात प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक को लागू करने का फैसला इसलिए किया है कि ताकि सुरक्षा और यात्री अनुभव को बेहतर बनाया जा सके. ये स्टेशन देश से सबसे बड़े और भीड़भाड़ वाले स्टेशन हैं- जैसे नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, हावड़ा आदि. इन स्टेशनों की सुरक्षा के मद्देनजर ही इस तकनीक को लागू किया जा रहा.
रेलवे स्टेशन भीड़भाड़ वाले स्थान होते हैं, जहां चोरी, आतंकवादी गतिविधियां या अन्य अपराध होने की आशंका रहती है. फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करती है, खासकर उन लोगों की जो अपराधी डेटाबेस में दर्ज हैं. यह तकनीक संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और अपराधियों को पकड़ने में सहायक है, जिससे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ती है.
टिकट चेकिंग और बोर्डिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जिससे यात्रियों को लंबी कतारों से बचाया जा सकता है. रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट स्टेशन बनाने की योजना के तहत यह तकनीक लागू की जा रही है, जिसमें सुरक्षा, निगरानी, और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है.
सवाल – क्या भारत में इस तकनीक के लिए आधार को भी डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा?
– भारत में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक (FRT) को आधार डेटाबेस के साथ जोड़कर उपयोग करने की संभावना निश्चित रूप से मौजूद है लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है. हालांकि भारत के पास आधार का जो डेटाबेस है वो बहुत जबरदस्त और बड़ा है. इसमें 1.3 अरब से अधिक नागरिकों का डेटा (उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों की स्कैन और चेहरा) शामिल है.
ये डेटाबेस FRT को सहायता भी कर सकता है.
आधार डेटाबेस में प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति की तस्वीर संग्रहित होती है. फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इस डेटा का उपयोग करके व्यक्तियों की पहचान कर सकता है, खासकर जब इसे अन्य डेटा (जैसे सीसीटीवी फुटेज) के साथ मिलान किया जाता है.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (AFRS) को लागू करने की योजना बनाई है, जो अपराधियों और लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आधार डेटाबेस के साथ जुड़ सकता है. हालांकि UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार डेटा का उपयोग केवल विशिष्ट परिस्थितियों में और कानूनी अनुमति के साथ ही किया जा सकता है.
दिल्ली पुलिस और अन्य राज्य पुलिस बलों ने FRT का उपयोग करके आधार डेटा के साथ संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की है, विशेष रूप से लापता बच्चों और अपराधियों की खोज में.
सवाल – क्या भारत का कानून फेशियल रेकॉग्निशन तकनीक के इस्तेमाल को आधार डेटाबेस के साथ जोड़ने की अनुमति देता है?
– आधार अधिनियम, 2016 के तहत आधार डेटा का उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्यों (जैसे सरकारी योजनाओं के लिए प्रमाणीकरण) के लिए किया जा सकता है. FRT के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए विशेष अनुमति और कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है. UIDAI ने कहा था कि आधार डेटा का उपयोग FRT के लिए तभी किया जा सकता है, जब यह प्रमाणीकरण प्रक्रिया का हिस्सा हो, न कि सामान्य निगरानी के लिए.
सवाल – फेशियल रेकॉग्निशन का फायदा क्या है, इससे किस तरह मदद मिलती है?
– यह तकनीक अपराधियों, वांछित व्यक्तियों, या संदिग्धों की तुरंत पहचान कर सकती है, जिससे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ती है. टिकट चेकिंग और पहचान सत्यापन में समय की बचत होती है, जिससे यात्रियों का अनुभव बेहतर होता है. मैनुअल निगरानी की तुलना में यह तकनीक अधिक सटीक और तेजी से काम करती है. संदिग्ध गतिविधियों को शुरुआती चरण में ही पहचानकर अपराध को रोका जा सकता है. यह तकनीक यात्री प्रवाह को समझने और स्टेशन प्रबंधन को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है.
सवाल – इस तकनीक पर लोगों ने लगातार चिंता भी जताई है. क्या इसके नुकसान भी हैं?
– इससे लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन होता है. फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक यात्रियों की निजी जानकारी को संग्रहित और उपयोग करती है, जिससे गोपनीयता के उल्लंघन की चिंता बढ़ती है.
फिर ये तकनीक हमेशा 100% सटीक नहीं होती. खराब रोशनी, चेहरे का मेकअप, या तकनीकी त्रुटियों के कारण गलत पहचान हो सकती है, जिससे निर्दोष लोगों को परेशानी हो सकती है. डेटाबेस में संग्रहित चेहरों की जानकारी अगर हैक हो जाए या दुरुपयोग हो, तो यह गंभीर समस्या हो सकती है. इस तकनीक को लागू करने और मेंटेन करने की लागत बहुत अधिक है, जिसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर पड़ सकता है.
सवाल – भारत में ये तकनीक कहां कहां लागू है?
– भारत में ये तकनीक अब तक हवाईअड्डों पर आमतौर पर लागू है. दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा पहल के तहत, फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग यात्री पहचान और बोर्डिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जा रहा है. ये यात्रियों को बिना कागजी टिकट या आईडी चेक के हवाई अड्डों पर प्रवेश और बोर्डिंग की सुविधा देता है. जुलाई 2019 में कुछ भारतीय हवाई अड्डों पर इस तकनीक को लांच किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने लापता बच्चों और अपराधियों की पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग शुरू किया है. 2019 में ट्रायल के दौरान इस तकनीक की मदद से लगभग 3,000 लापता बच्चों की पहचान की गई. NCRB ने ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (AFRS) से अपराधियों की पहचान और निगरानी के लिए लागू करने की दिशा में काम किया है. यह तकनीक सीसीटीवी फुटेज और डेटाबेस के साथ मिलान करके अपराध नियंत्रण में मदद करती है.
दिल्ली और चेन्नई में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल, सार्वजनिक स्थानों और अन्य क्षेत्रों में निगरानी के लिए भी हो रहा है. यह तकनीक पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों को तेजी से ट्रैक करने में मदद करती है.
कुछ स्कूलों और कॉलेजों में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग अटेंडेंस ट्रैक करने और गैरहाजिर छात्रों की पहचान के लिए किया जा रहा है. कुछ बैंकों में ग्राहक सत्यापन और सुरक्षा के लिए इस तकनीक का उपयोग शुरू हो रहा है.
सवाल – चीन ने किस तरह बहुत बड़े पैमाने पर इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है?
– हां, चीन इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है. चीन में चौराहों और सड़कों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाता है. 2018 तक चीन में 170 मिलियन से अधिक सीसीटीवी कैमरे थे. 2020 तक इसे बढ़ाकर 400 मिलियन करने की योजना थी.
इन कैमरों का उपयोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और सामाजिक व्यवहार को ट्रैक करने के लिए किया जाता है. चीन की “शार्प आइज़” परियोजना के तहत, चौराहों, सड़कों, शॉपिंग मॉल, और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कैमरों को एकीकृत करके एक राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क बनाया गया है. यह नेटवर्क फेशियल रिकॉग्निशन और AI का उपयोग करके नागरिकों की गतिविधियों को ट्रैक करता है.
चौराहों के अलावा चीन में FRT का उपयोग बैंकों, हवाई अड्डों, होटलों यहां तक कि सार्वजनिक शौचालयों में भी किया जाता है.

 5 hours ago
5 hours ago







)

)