पुणे के लोग इस बात पर फख्र करते हैं कि उनके शहर में सबसे पहले पाइपलाइन और नलों के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचा. उस समय के लिहाज से ये किसी सपने जैसा था. आखिर वो क्या बात थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने पुणे को ऐसा पहला शहर बना दिया, जहां 140 साल पहले नलों से घरों तक पानी पहुंचा दिया गया. वहां के लोगों को इसके बाद नदियों, तालाबों और कुंओं से जाकर पानी भरकर लाने के मुश्किल काम से निजात मिल पाई.
भारत में पुणे पहला शहर था, जहां नल से साफ पानी घरों तक पहुंचा. आज बेशक घरों में नल की टोंटी खोलते ही पानी आना एक साधारण काम लगता हो लेकिन कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था. उन्नीसवीं सदी के आखिर में ये एक क्रांतिकारी बदलाव था. आखिर क्यों ब्रिटिश राज के लोगों ने पुणे को ही नल के पानी पहुंचाने के लिए पहले शहर के तौर पर चुना.
अंग्रेज़ों के आने से पहले पुणे का पानी मुख्य रूप से कुओं, बावड़ियों और तालाबों से आता था. बरसात में पानी खराब यानि प्रदूषित हो जाता था. ये गंदा पानी रोग फैलाने वाला साबित होता. तब हैज़ा, टाइफॉयड और डायरिया जैसी बीमारियां आम थीं.
पुणे कैंट में प्रदूषित पानी से होने लगीं बीमारियां
1817 में जब पुणे पर ब्रिटिशों का अधिकार हुआ और यहां कैंटोनमेंट बना, तो समस्या गंभीर हो गई. हज़ारों सैनिकों और उनके परिवारों को साफ पानी चाहिए था. कुओं और तालाबों पर निर्भर रहना मुश्किल था. कैंट एरिया में रहने वाले अंग्रेज अफसरों, सैनिकों और उनके परिवारों में पानी से संबंधित बीमारियां आम होने लगीं. इससे उन्हें बहुत दिक्कत होती थी. 19वीं सदी में पुणे शिक्षा, प्रशासन और सैन्य गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन चुका था. यहां भारतीय एलीट वर्ग और ब्रिटिश अफ़सर दोनों बसते थे, जिन्हें आधुनिक सुविधाएं चाहिए थीं.
वर्ष 1850 के आसपास का पुणे शहर, जहां शहर के लोगों को पानी के लिए कुओं, नदी और तालाबों पर रहना पड़ता था.
तब बनी पाइप लाइन से साफ पानी पहुंचाने की योजना
इसके बाद ये सोचा जाना लगा कि आखिर कैंटोनमेंट तक साफ पानी कैसे पहुंचाया जाए. इसके बाद अंग्रेज ये सोचने लगे कि क्या पाइप लाइन के जरिए वहां तक साफ पानी भेजा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज ये काम इंग्लैंड में बखूबी कर चुके थे.
इसके चलते ब्रिटिश इंजीनियरों ने 1870 ये योजना बनाई कि कैसे पानी पुणे कैंटोनमेंट तक पाइपलाइन से लाया जाए. इसके पहले चरण में बांध बनाना था, जहां पानी को स्टोर कर सकें. फिर इसके बाद पाइपलाइन के जरिए इसको शहर तक पहुंचाया जाए.
1873 में मुठा नदीं पर बांध का काम शुरू हुआ. 1879 तक खडकवासला डैम तैयार हो गया. इसे बनाने में करीब 6 साल लगे. यह बांध उस समय के लिए इंजीनियरिंग का अजूबा था. पत्थर और चूना-गारे से बनी विशाल दीवार ने पानी को रोका. बांध की लागत करीब 50 लाख रुपये आई, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी.
पानी को शहर से 20 किलोमीटर दूर से पाइप से लाना था
बांध बनने के बाद असली चुनौती शुरू हुई कि पानी को वहां से 20 किलोमीटर दूर पुणे शहर तक कैसे पहुंचाया जाए. इंजीनियर कर्नल आर.एस. कैपल और जे.एच.सी. फिंडक्ले को यह काम दिया गया.
यह परियोजना भारत में पहली बार “ग्रेविटी बेस्ड” पाइपलाइन सिस्टम का उदाहरण बनी. यानी ऊंचाई से नीचे की ओर पानी अपने दबाव से बहकर घरों तक पहुंचता था.
उस समय भारत में इतनी मज़बूत पाइपें नहीं बनती थीं. इसलिए लंदन से भारी लोहे की पाइपें मंगाई गईं. इन्हें समुद्र के रास्ते बंबई (मुंबई) और वहां से बैलगाड़ियों के जरिये पुणे तक लाना पड़ा.
पाइप बिछाना तो बिल्कुल आसान नहीं था
खडकवासला से पुणे तक का इलाका टेढ़ा-मेढ़ा और ऊबड़-खाबड़ था. वहां पाइप बिछाना आसान नहीं था. कई जगह चट्टानें काटनी पड़ीं. जो मजदूर इस काम में लगाए गए, उन्हें गर्मी, बीमारियाँ और भारी काम की वजह से काफी दिक्कतें हुईं. वो बार बार बीमार पड़ते. कई मजदूरों की मौत भी हुई. लगातार कठिनाइयों के बावजूद इंजीनियरों ने 1880 के दशक की शुरुआत तक यह काम पूरा कर लिया.
मुठा नदी पर अंग्रेजों द्वारा 1879 में बनाया गया बांध. (फाइल फोटो)
…और फिर पानी नलों से घरों तक पहुंचा
जब पहली बार पानी पाइप से लोगों के घरों और सार्वजनिक नलों तक पहुंचा, तो शहर में उत्साह और आश्चर्य दोनों देखने को मिले. अमीर और पढ़े-लिखे पुणे वासी इसे आधुनिक सुविधा मानकर बहुत खुश हुए. उनके लिए ये यूरोप जैसा अनुभव था.
परंपरावादियों और ब्राहणों ने इस पानी का विरोध भी किया
गरीब तबके और परंपरावादियों ने जरूर में इसका विरोध किया, क्योंकि उनमें इसे लेकर शुरू में अविश्वास था. कुछ लोगों को डर था कि पाइप का पानी अपवित्र है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह पानी कहां से आता है. कई ब्राह्मण परिवारों ने शुरू में पाइप का पानी पीने से मना कर दिया. अपने कुओं से ही पानी लाने पर जोर दिया.
नल का पानी पुणे के गर्व का प्रतीक बन गया
इस पाइप लाइन से जब पानी आने लगा तो बीमारियां कम होने लगीं. ये पानी की सुविधा भी आसान थी. लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया. कहा जाता है कि 1890 के दशक तक पुणे में नल से पानी आना गर्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया. आमतौर पर 1886 में पुणे में लोगों के घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचने लगा.
पुणे बना भारत का ‘आधुनिक पानी’ वाला पहला शहर
शुरू में यह सुविधा केवल कैंटोनमेंट, ब्रिटिश बंगलों और चुनिंदा अमीर भारतीय परिवारों तक सीमित थी. बाद में नगरपालिकाओं ने धीरे-धीरे आम नागरिकों के मोहल्लों में भी नल लगाए. इस बदलाव का असर काफी बेहतर रहा. हैज़ा और टाइफॉयड के प्रकोप घटने लगे. लोगों का समय और मेहनत बची. खासकर महिलाओं का जो कुओं से पानी भरने जाती थीं. पुणे को ‘भारत का पहला आधुनिक पानी वाला शहर’ कहकर पहचाना जाने लगा.
फिर ऐसे प्रोजेक्ट दूसरे शहरों के लिए शुरू हुए
इसके बाद मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में भी इसी तरह की परियोजनाएं शुरू हुईं. वहां भी नलों के जरिए घरों तक पानी पहुंचाया गया. कहा जाता है कि जब पहली बार शहर में सार्वजनिक नल खोला गया, तो लोग घंटों तक वहां खड़े होकर पानी की धार को निहारते रहे. कई बच्चों ने पाइप से निकलते पानी को देखकर तालियां बजाईं. उस समय के समाचार पत्रों ने इस घटना को “भारत की आधुनिकता की ओर पहला कदम” बताया.
रोमन साम्राज्य में अमीरों के घर यूं पहुंचता था पानी
रोमन साम्राज्य के दौरान रोम और अन्य रोमन शहरों में एक्वाडक्ट्स से पानी लाकर पत्थर और सीसे की पाइपों के जरिये अमीर घरों और सार्वजनिक स्नानगृहों तक पहुंचाया जाता था. कई घरों में नल जैसी कांस्य की फिटिंग्स लगी थीं.
लंदन में लगा था पहला आधुनिक पाइपलाइन सिस्टम
लंदन में 1609 में पहली बार न्यू रिवर कंपनी ने लकड़ी की पाइपों से पानी सप्लाई करना शुरू किया. अमीर घरों तक नल और पाइप से पानी पहुंचने लगा. फिलाडेल्फिया में 1801 में पहला मॉडर्न म्युनिसिपल वॉटर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया. जहां शहर के नागरिकों के लिए संगठित पाइपलाइन नेटवर्क बनाया गया. 1800 के दशक में नेपोलियन के आदेश पर यहां भी आधुनिक वॉटर पाइपलाइन सिस्टम बना.
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

 1 month ago
1 month ago




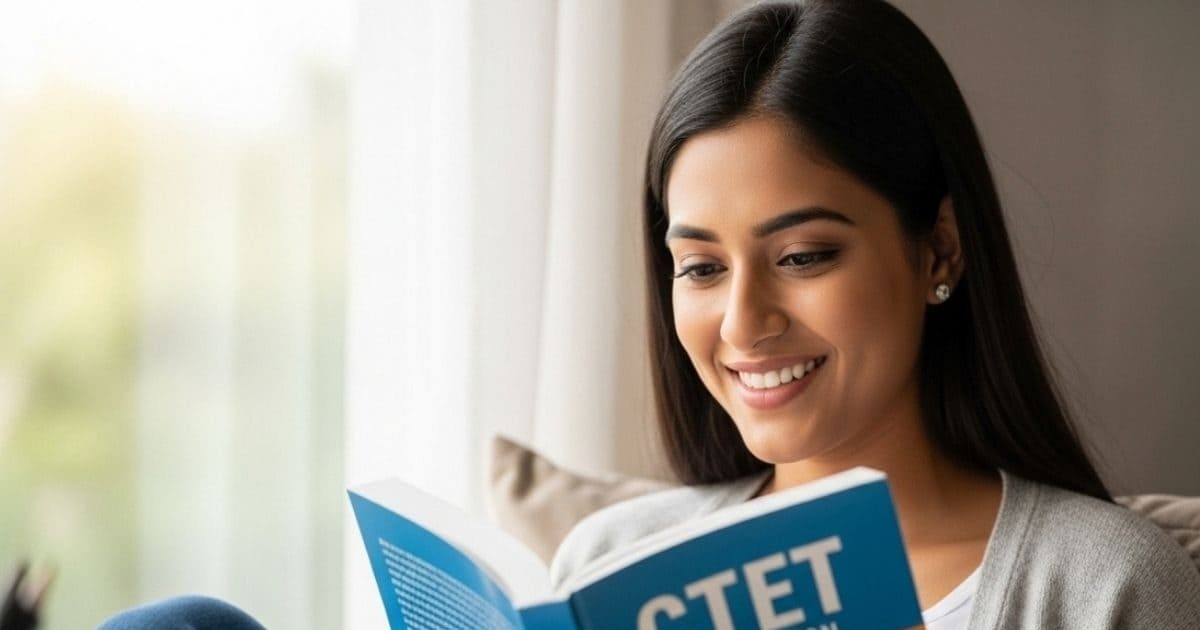








)

)
